Pollution, Natural Disasters and Management को एमपीपीएससी प्रीलिम्स के यूनिट-7 के अंतर्गत हमलोग सबसे पहले प्रदूषण को विस्तृत रूप में पढ़ेंगे।
प्रदूषण- वातावरण के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक अवस्था में ऐसा परिवर्तन, जिसमें मानव, जीव-जंतु, वनस्पति तथा नैसर्गिक कारकों को हानि पहुंचे, प्रदूषण कहलाता है। अर्थात् कुछ प्रदूषित पदार्थों का वातावरण में घुलकर उसके भौतिक रासायनिक एवं जैविक अवस्था में परिवर्तन, पदूषण कहलाता है। पर्यावरण के बढ़ते पदूषण के कारण मानव के जीवन पर विपरीत असर पड़ने के कारण विश्वभर के देशों का पहला पर्यावरण सम्मेलन 1972 ई. में सयुक्ंत राष्ट्र के स्टॉक होम, स्वीडन में सम्पन्न हुआ। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, एक सांविधिक संगठन है। इसका गठन जल, प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम, 1974 के अधीन सितंबर, 1974 ई. में किया गया था। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को वायु अधिनियम, 1981 के तहत शक्तियां और कार्य सौपे गये।
प्रदूषण के प्रकार-
प्रदूषण को विभिन्न आधारों पर विभाजित किया जा सकता है-
- प्रदूषकों की उत्पत्ति के आधार पर– इसके आधार पर दो प्रकार के होते हैं-
- प्राथमिक प्रदूषक- वह जो स्त्रोत से सीधे निकलकर पर्यावरण के घटकों में मिलकर नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे- कार्बन मोनो आक्साइड, सल्फरडाई आक्साइड, नाइट्रोजन के आक्साइड आदि।
- द्वितीयक प्रदूषक– जब प्राथमिक प्रदूषक के घटक, पर्यावरण के किसी भी घटक से रासायनिक अभिक्रिया करते हैं और नया यौगिक बनाते हैं और नुकसान पहुचाते हैं। जैसे- So3, Hno3, H2So4, O3 and PAN etc.
- पर्यावरण के भागों या कारकों के आधार पर-
- वायु प्रदूषण
- जल प्रदूषण
- ध्वनि प्रदूषण
- मृदा प्रदूषण और
- रेडियो एक्टिव प्रदूषण।
Pollution Natural Disasters and Management
वायु प्रदूषण-
वायुमण्डल में उपस्थित गैसों कार्बनडाईआक्साइड, नाइरट्रोजन, आक्सीजन आदि के निश्चित अनुपात में अवांछनीय परिवर्तन, वायुप्रदूषण कहलाता है। वायुप्रदूषण के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं-
- मानव के क्रियाकलापों से निष्काशित गैसें व धुंआ, कणकीय पदार्थ व ऊष्मा आदि।,
- जैवकि पदार्थों के सड़ने व गलने से निकलने वाली गैसें जैसे सल्फरडाईआक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड व ज्वालामुखी विस्फोट तथा जंगल में आग लगने के कारण आदि।
- सल्फर डाईआक्साइड, कार्बन मोनोआक्साइड
वायु प्रदूषण से संबंधित रोग
सिलिकोसिस- यह रोग सांस के साथ सिलिकॉन और सिलिकॉन डाइऑक्साइड के जाने से होता है। सामान्यत: यह रोग खनिज पोल्टी उद्योग, कांच उद्योग, भवन निर्माण में कार्यरत लोगों को होता है।
पलम्बिस– यह रोग वायु में शीशे की मात्रा के अधिक होने से होता है। इसमें भ्रम, पागपन व लीवर की क्षति आदि रोग होते हैं।
वायु प्रदूषण के प्रभाव-
अम्लीय वर्षा- सल्फर एवं नाइट्रोजन के आक्साइड , सल्फ्यूरिक अम्ल एवं नाइट्रिक अम्ल एवं कार्बन डाइ आक्साइड से कार्बनिक अम्ल मिलकर अम्लीय वर्षा करते हैं।
फ्लाई एश- बिटूमिनस कोयले के दहन से तापीय विद्युत घरों में उत्पन्न होती है। यह प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करती है। तथा ब्रोंकाइटिस, फेफडों का कैंसर वसिलिकोसिस नाम की बीमारी उत्पनन करती है।
पार्टिकुलेट मैटर –
- वायुमण्डल में उपस्थित अतिसूक्ष्म कण जो ठोस व तरल अवस्था में पाये जाते हैं, पीएम कहलाते हैं।
- पीएम 10 का अर्थ है वह कण जिनका व्यास 10 माइक्रोमीटर होता है।
- पीएम 2.5 वाले सूक्ष्म कण मानव के फेफडों में पहुचकर अधिक नुकसान पहुचाते हैं।
- वायुमंडल में इनकी मात्रा बढने से धुंध और मनुष्य में श्वास संबंधी बीमारियां, आखों में जलन और कैंसर जैसी बीमारियां हो जाती है।
- पीएम 2.5 की मात्रा 60 और पीएम 10 की मात्रा 100 होने तक हवा को सांस लेने के लिये सुरक्षित माना जाता है।
Pollution Natural Disasters and Management (राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक)-
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वायु की गुणवत्ता की निगरानी करने और जरूरी कार्यवाही करने के लिये देश के बड़े शहरों में रियल टाइम के आधार पर प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक का शुभारंभ किया गया।
- गुणवत्ता सूचकांक में वायु की मुख्यत: 06 श्रेणियां है- अच्छी, संतोषजनक, सामान्य, खराब, बहुत खराब और गंभीर।
- वायु गुणवत्ता सूचकांक में 08 प्रदूषणकारी तत्वों पर किया जाता है, वह हैं- पीएम 10, पीएम 2.5, नाइट्रोजन डाइ आक्साइड, ओजोन, अमोनिया, सल्फरडाई आक्साइड, कार्बन मोनोक्साइड तथा लेड ।
वायु प्रदूषण (निरोध एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981– यह अधिनियम मुख्य रूप से वायु प्रदूषण को नियन्त्रित रखन के लिये बनाया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षण प्रदान करना है।
जल प्रदुषण- जल में किसी प्रकार का अवांछनीय, गैसीय, द्रवीय या ठोस पदार्थों का मिलना, जल प्रदूषण कहलाता है। जल प्रदूषण के प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं-
- समुद्री जल प्रदूषण।
- नदी जल प्रदूषण
- झील जल प्रदूषण
- भूमिगत जल प्रदूषण
- तापीय जल प्रदूषण
- सतही जल प्रदूषण
जल प्रदूषण के प्रभाव-
जल मुख्यत: जलीय जीव-जंतु, मानव, वनस्पति आदि सभी के लिये आवश्यक है। अत: जल प्रदूषण का प्रभाव भी इन सभी पर पड़ता है।
प्रबंधन या नियंत्रण-
- जल प्रदूषण के संबध में लोगों को जागरूक करना चाहिये।
- आम लोगों को कूडा-कचड़े के प्रबंधन में दक्ष करना चाहिये।
- कारखानों से निकलने वाले अपशिष्ट के लिये स्पष्ट नियम बनाये जाने चाहिये।
- नगरपालिकाओं के लिये सीवर शोधन संयंत्रों की व्यवस्था कराई जानी चाहिये।
जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम, 1974 – वर्ष 1974 में भारत सरकार ने जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम को पारित करके जल प्रदूषण की रोकथाम के लिये पहल की थी, जिसे 1988 ई. में संशोधित किया गया। इस अधिनियम का उद्देश्य- मानव उपयोग के लिये जल की गुणवत्ता को बनाए रखना है।
Pollution Natural Disasters and Management
ध्वनि प्रदूषण- ध्वनि जब एक निश्चित सीमा से अधिक हो जाती है, तो वह मानव व जीव-जंतुओं के लिये घातक हो जाती है, तब उसे ध्वनि प्रदूषण कहते है। एक सामान्य व्यक्ति के लिये ध्वनि की तीव्रता 50 डेसीबल से 80 डेसीबल के मध्य में होना चाहिये।
- ध्वनि प्रदूषण के कारण- इसके मुख्यत: दो कारण होते हैं-
- प्राकृतिक कारण- इसमें भूकंप की ध्वनि, तेजी से गिरते पानी की ध्वनि, बिजली का तडकना, बादलों का गर्जना आदि कारक होते हैं।
- मानवीय कारक- मानव मुख्यत: आवागमन के साधनों के द्वारा, कारखानों के शोर-शराबे से और सामाजिक क्रियाकलापों तथा मनोंरंजन के साधनों से ध्वनि प्रदूषण को बढावा देता है।
प्रभाव-
- अधिक शोर के कारण मानव के कानों की श्रवण शक्ति स्थायी और अस्थायी रूप से खत्म हो जाती है।
- अत्यधिक शोर के कारण मानव स्वभाव से चिंतित, चिढचिढा और तनावग्रस्त हो जाता है।
- उच्च ध्वनि से मानवों में उच्च रक्त चाप, माइग्रेन, पेट का उल्सर, अनिद्रा आदि बीमारियां हो जाती है।
- तीव्र ध्वनि से सूक्ष्म जीवाणु मर जाते हैं, जिससे मृत अवशेषों के अवघटन में बाधां उत्पन्न होती है।
नियंत्रण-
- सड़कों के आसपास वृक्षारोपण करके ध्वनि प्रदूषण को कम किया जा सकता है।
- तीव्र ध्वनि क्षेत्रों में ग्रीन बेल्टों का निर्माण करके ।
- मानव द्वारा तीव्र ध्वनि क्षेत्रों में सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करके।
- वाहनों में साइलेंसर का उपयोग करके।
मृदा प्रदूषण– मानव या किसी जीव-जंतु द्वारा मृदा की गुणवत्ता में नुकसान पहुंचाना, मृदा प्रदूषण कहलाता है। मृदा प्रदूषण के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं-
- घरों से निकले वाले कूड़ा-करकट तथा अपशिष्ट पदार्थों के मिलने से मृदा प्रदूषित हो जाती है।
- फसलों में कीटनाशी व खरपतवार नाशी के प्रयोग से मृदा प्रदषित हो जाती है।
- अत्यधिक समय तक एक स्थान पर जल भराव के कारण मृदा प्रदूषित हो जाती है।
प्रभाव-
- मृदा के प्रदूषण से मिट्टी के मौलिक गुणों में हृास होता है, जिससे उसक उत्पादक क्षमता कम हो जाती है।
- कीटनाशकों के प्रयोग से मृदा के भौतिक व रासायनिक गुणों में हृास होता है।
- प्रदूषित मृदा में उत्पन्न होने वाली खाद्यान फसलें मानव शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं।
नियंत्रण/प्रबंधन-
- खाद के रूप में गोबर, पत्तों का खाद व रासायनिक खाद का प्रयोग कम करना चाहिये।
- जैविक खाद का प्रयोग अधिक मात्रा में किया जाना चाहिये।
- फसलों का उत्पादन करने के लिये कम से कम कीटनाशकों का प्रयोग किया जाना चाहिये।
- कारखानों से निकलने वाले कचड़े को जमीन के अंदर दबा देना चाहिये।
रेडियोधर्मी प्रदूषण-
रेडियोएक्टिव पदार्थों से निकलने वाले विकरणों से होने वाले प्रदूषण को रेडियोधर्मी प्रदूषण कहते हैं। जैसे- यूरेनियम, थोरियम व प्लूटोनियम आदि। रेडियोधर्मी प्रदूषण के मापन की इकाई रोण्टजन है। रेडियोधर्मी प्रदूषण मुख्यत: दो प्रकार का होता है-
- मानवजनित- परमाणु बमों के विस्फोट, प्लूटोनियम व थोरियम का शुद्धिकरण, आण्विक ऊर्जा संयंत्र आदि से होने वाला प्रदूषण।
- प्रकृति जनित- पृथ्वी पर पाये जाने वाले रेडियोएक्टिव पदार्थों के निष्कर्षण व सूर्य की किरणों के कारण जो प्रदूषण होता है, वह प्रकृति जनित प्रदूषण कहलाता है।
प्रभाव-
- इसके प्रभाव के कारण मनुष्य में खतरनाक रोग जैसे- हड्डी कैंसर, रक्त कैंसर व क्षय रोग आदि हो जाते हैं।
- जीन और गुणसूत्रों में हानिकारक परिवर्तन हो जाते हैं।
- परमाणु बमों के विस्फोट ने जापान के हिरोशिमा व नागाशाकी शहरों को तबाह कर दिया था।
नियंत्रण / प्रबंधन-
- समुद्र, नदी व जल में रेडियोएक्टिव पदार्थों को विसर्जित नहीं किया जाना चाहिये।
- परमाणु रिएक्टरों की स्थापना मानव आबादी क्षेत्रों से दूर की जानी चाहिये।
- मानव प्रयोग के उपकरणों को रेडियोधर्मिता से मुक्त किया जाना चाहिये।
- परमाणु अस्त्रों का उत्पादन व उपयोग पूर्णत: वर्जित होना चाहिये।
प्रकृति और मात्रा के आधार पर-
- मात्रात्मक प्रदूषक- वातावरण में उपस्थित गैसों की मात्रा के बढने से नुकसानदायक जैसे- कार्बनडाई आक्साइड, मीथेन आदि ।
- गुणात्मक प्रदूषण– वह, जिनकी उपस्थिति ही पर्यावरण को नुकसानदायक होती है। सामान्यत: मानव द्वारा निर्मित होते हैं। जैसे- डीटीसी, कीटनाशक आदि।
पारिस्थितिकी तंत्र के आधार पर-
जैव निम्नीकरणीय (biodegradable)- वह प्रदूषक जो समय के साथ प्रकृति में सरलता से हानि रहित तत्वों में विघटित हो जाते हैं। जैसे- पशुओं का मल मूत्र, सीवेज और घर का कूडा-करकट आदि।
जैव निम्नीकरणीय रहित(Non-biodegradable)- वह प्रदूषक, जिनका या तो अपघटन नहीं होता है या फिर अपघटन बहुत धीरे-धीरे होता है। यह साधारणत: मनुष्यों द्वारा निर्मित होते हैं। जैसे- डीडीटी, पालीथीन, प्लास्टिक डिब्बे आदि।
Pollution Natural Disasters and Management (प्राकृतिक आपदाएं)-
प्राकृतिक तौर पर घटित होने वाली ऐसी घटनाएं जिनसे जान-माल की हानि होती है, प्राकृतिक आपदाएं कहलाता है। प्राकृतिक आपदाएं मुख्यत: तीन प्रकार की होती हैं-
- वायुजनित- तूफान, तेजहवाएं, चक्रवात
- जलजनित- बाढ़, सूखा, बादल फटना।
- धरती जनित- भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी।
बाढ़- जब एक निश्चित क्षेत्र में सामान्य से अधिक जल जमा हो जाये, जिससे जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो जाये, तो इस स्थिति को बाढ़़ कहते है। बाढ आने के प्रमुख कारण निम्न है-
- प्राकृतिक कारण-नदियों द्वारा, अधिक वर्षा के कारण, बादलों का फटना, हिमानी का पिघलन।
- मानवनिर्मित कारण- तटों पर मानव वस्तियों के कारण, वनों का काटना, अनुचित प्रबंधन, बांध टूटने के कारण।
प्रभाव-
- बाढ मुख्यत: दो प्रकार से मानव को प्रभावित करते हैं-
- प्रत्यक्ष- जानमाल की हानि, रेल पटरियों का ध्वस्त होना, सडकें बाधित आदि।
- अप्रत्यक्ष- बीमारियों जैसे- डायरिया, हैजा व पीलिया आदि का फैलना।
प्रबंधन-
- बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का चिन्हांकन किया जाना चाहिए।
- निर्माण कार्य की अनुमति नहीं देनी चाहिये।
- नदियों के तटों को चौड़ा करना चाहिये।
- वृक्षारोपड़ किया जाना चाहिये।
- मौसम संबंधी सूचनाओं के प्रति जागरूक होना चाहिये।
Pollution Natural Disasters and Management (सूखा)-
सूखा- किसी क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा से 90 प्रतिशत से कम वर्षा होने की स्थिति को सूखा कहा जाता है। सूखा की स्थिति उत्पन्न होने के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं-
- वनों का हृास।
- ग्रीन हाउस प्रभाव ।
- एलनीनों आने के कारण।
प्रभाव-
- जलसंकट की स्थिति उत्पन्न होना।
- कृषि कार्य पूरी तरह नष्ट हो जाता है।
- उद्योगों का बंद हो जाना।
- बेरोजगारी बढ़ जाती है, तो लोग पलायन करने लगते हैं।
प्रबंधन-
- वृक्षारोपण किया जाना चाहिये ।
- भू-जल का संरक्षण किया जाना चाहिये।
- बड़े बडे बांध का निर्माण किया जाना चाहिये।
- कृषि में ड्रिप सिंचाई का उपयोग करना चाहिये।
Pollution Natural Disasters and Management (भूकंप)-
- यह दो शब्दो भू और कंप से बनता है। अर्थात। पृथ्वी का कांपना।
- पृथ्वी की ऊपरी सतह का कांपना ही भूकंप कहलाता है। भूकंप आने के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं-
- प्राकृतिक कारण- उल्का पिण्ड के गिरने से, ज्वालामुखी आने से, चटटानों की बलन क्रिया से एवं भूस्खलन से आदि।
- मानवीयकृत कारण- परमाणु परीक्षण के समय, खदानों से, बडे-बडे बांधों के बनने से,
प्रभाव-
- सभी प्राकृतिक आपदाओं में भूकम्प का सबसे अधिक प्रभाव पडता है, जो कि निम्नलिखित है-
- जान-माल की क्षति- यहद रिक्टर पैमाने पर भूकम्प की तीव्रता 6 या इससे अधिक हो, तो जान-माल की अपार क्षति होती है।
- 26 जनवरी, 2001 को कच्छ में आए भूकम्प से गुजरात के भुज, भडौच, गांधीधाम मलवे के ढेर बन गए थे।
प्रबंधन-
- समान भूकंप क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा खींचनी चाहिये।
- भूकंप का मापन रिक्टर स्केल पर मापा जाना चाहिये।
- भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में ऊचीं इमारतो, बडे औद्योगिकों को बढावा न देना चाहिये ।
- जन-जागरूकता तथा शैक्षिक अभियानों द्वारा भूकम्प के खतरों के प्रति जनता को सचेत किया जाना चाहिये।
Pollution Natural Disasters and Management (अन्य प्रमुख तथ्य)-
- मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण, ऐन्थ्रोपोजेनिक प्रदूषण कहलाता है।
- वाहित मल या सीवेज जैव विघटित प्रदूषक है।
- ओजोन एक द्वितीयक प्रदूषक है।
- सल्फर डाइआक्साइड श्वसन प्रणाली के एंजाइम्स को प्रभावित करती है व एलर्जी, दमा आदि की समस्या प्रकट करती है।
- नाइट्रोजन ऑक्साइड आक्सीजन तथा ओजोन से मिलकर पेरोक्सीएसिटिल नाइट्रेट (पेन) का निर्माण करती है।
- एमीशन नॉर्मस पर्यावरण और वन-जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आता है।
Pollution Natural Disasters and Management

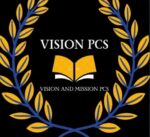
Pingback: Arts and Architecture of MP
Pingback: Narmadapuram Division । नर्मदापुरम् संभाग । - VISION PCS